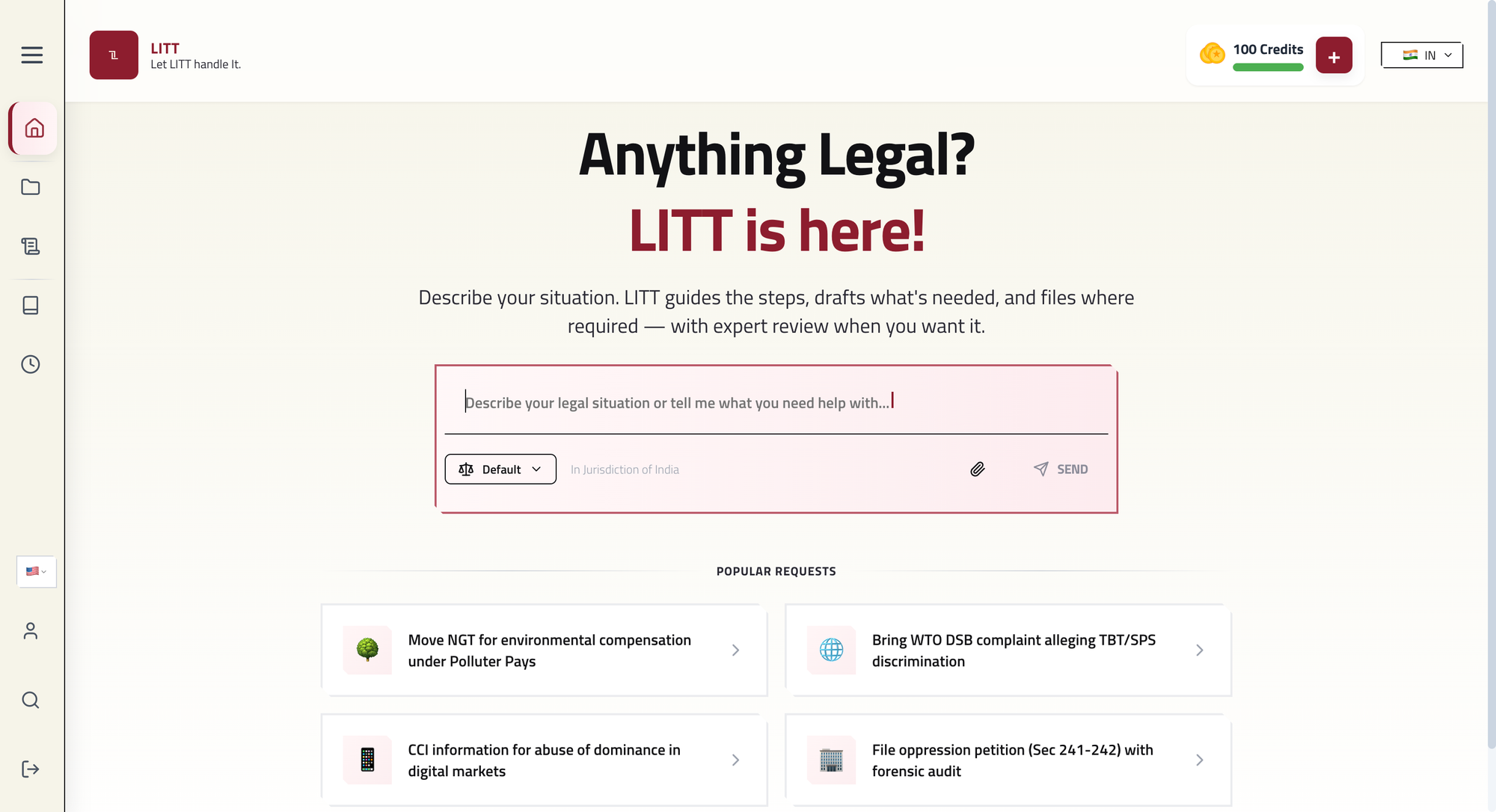स्थानांतरण संपत्ति अधिनियम, 1882 की धारा 52 के तहत लिस पेंडेंस का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि लंबित न्यायिक विवाद में शामिल किसी संपत्ति का हस्तांतरण न हो, जिससे न्यायिक परिणामों की सुरक्षा हो और तीसरे पक्ष के अधिकारों का हस्तक्षेप न हो।
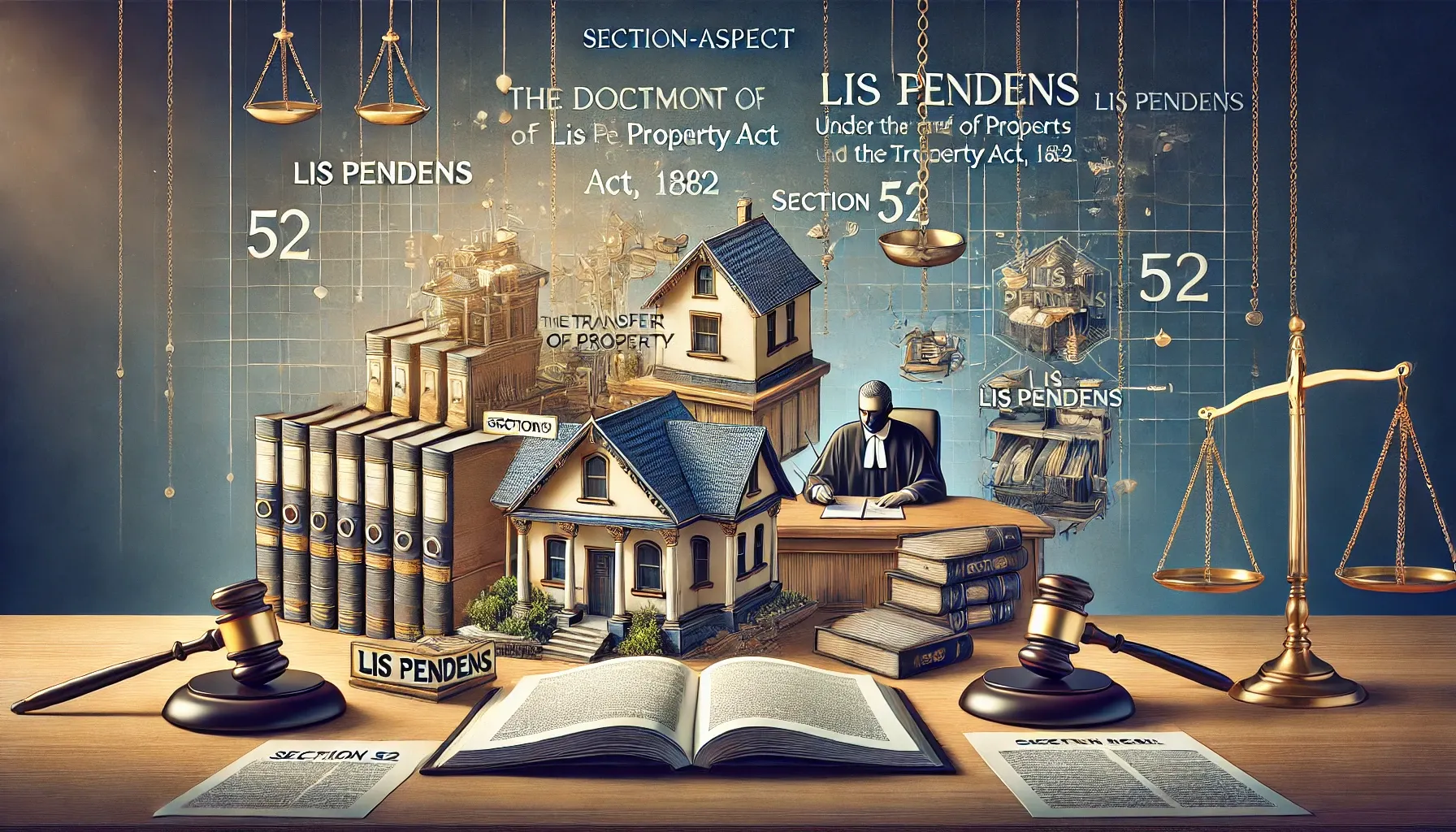
AI legal research and drafting tool
परिचय
लिस पेंडेंस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "लंबित मुकदमा"। यह एक कानूनी कहावत " पेंडेंटे लिटे निहिल इनोवेचर" पर आधारित है , जिसका अर्थ है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान कुछ भी नया पेश नहीं किया जाना चाहिए।
भारत में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (टीपीए) की धारा 52 के तहत लिस पेंडेंस का सिद्धांत निहित है । यह धारा किसी मुकदमे या कार्यवाही के लंबित रहने तक संपत्ति के हस्तांतरण के प्रभाव से संबंधित है। यह समानता और सार्वजनिक नीति पर आधारित है।
लिस पेंडेंस का सिद्धांत संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 के तहत
संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 लिस पेंडेंस के सिद्धांत को स्थापित करती है। यह धारा यह स्पष्ट करती है कि जब किसी संपत्ति के संबंध में कोई मामला अदालत में लंबित है, तो उस संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अधिकार या हस्तांतरण मान्य नहीं होगा।
धारा 52 के अनुसार:
- जब तक कोई मामला अदालत में लंबित है, तब तक उस संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का अधिकार का अंतरण या परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- यदि कोई व्यक्ति उस संपत्ति पर अधिकार का दावा करता है, तो उसे अदालत के निर्णय का इंतजार करना होगा।
- यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि विवादित संपत्ति के संबंध में कोई भी नया अधिकार या दावा तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि अदालत का निर्णय नहीं आ जाता।
- धारा 52 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान संपत्ति के अधिकारों में कोई परिवर्तन न हो, जिससे विवाद का समाधान होने तक स्थिरता बनी रहे।
- भारत की सीमाओं के भीतर या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी सीमाओं से परे स्थापित प्राधिकार वाले किसी न्यायालय में लंबित रहने के दौरान, कोई वाद या कार्यवाही, जो कपटपूर्ण न हो और जिसमें अचल संपत्ति का कोई अधिकार प्रत्यक्षतः और विशिष्टतः प्रश्नगत हो, वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा उस संपत्ति को इस प्रकार अंतरित या अन्यथा नहीं किया जा सकता है, जिससे उसमें पारित किसी डिक्री या आदेश के अधीन किसी अन्य पक्षकार के अधिकारों पर प्रभाव पड़े, सिवाय न्यायालय के प्राधिकार के और उसके द्वारा अधिरोपित शर्तों के अधीन।
- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी वाद या कार्यवाही का लंबित रहना, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में वादपत्र के प्रस्तुत किए जाने या कार्यवाही संस्थित किए जाने की तारीख से प्रारंभ माना जाएगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक कि वाद या कार्यवाही का अंतिम डिक्री या आदेश द्वारा निपटारा नहीं कर दिया जाता है और ऐसी डिक्री या आदेश की पूर्ण संतुष्टि या उन्मोचन प्राप्त नहीं कर लिया जाता है, या किसी समय प्रवृत्त विधि द्वारा उसके निष्पादन के लिए विहित परिसीमा अवधि की समाप्ति के कारण वह अप्राप्य नहीं हो जाता है ।
- विचाराधीन बाद का नियम जिस सिद्धान्त पर आधारित है उसे लार्ड जस्टिस टर्नर ने बेलामी बनाम सैवाइन[1]' नामक वाद में स्पष्ट किया था। उनके अनुसार यह सिद्धान्त इस मूल (foundation) पर आधारित है कि वह बिल्कुल ही असम्भव होगा कि किसी कार्यवाही या वाद को उसकी सफल परिणति (successful termination) तक ले जाया जायेगा। यदि वाद के लम्बित रहते हस्तांतरण की अनुमति दी जाय। वादी प्रत्येक मामले में प्रतिवादी द्वारा निर्णय या डिक्री से पूर्व अन्तरण करके निष्फल कर दिया जायेगा और वह (वादी) अपनी कार्यवाही को नये सिरे से प्रारम्भ करने के लिए मजबूर हो जायेगा और पुनः उसे वहीं कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस तरह इस धारा में अन्तर्विष्ट सिद्धान्त साम्या, शुद्ध अन्तःकरण और न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार है क्योंकि वे साम्यिक और न्यायोचित आधारशिला पर टिके हुये हैं।[2]
उद्देश्य
- इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब कोई मामला अदालत में लंबित हो, तो उस मामले से संबंधित संपत्ति पर किसी भी प्रकार का हस्तांतरण या अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। इससे यह सुनिश्चित होता है कि न्यायालय के निर्णय के बाद ही संपत्ति के अधिकार स्पष्ट हो सकें।
- लिस पेंडेंस के सिद्धांत के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत कानूनी कार्रवाई में शामिल पक्षों के अधिकारों की रक्षा करना और पक्षों को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान विवाद के विषय-वस्तु को इस तरह स्थानांतरित करने से रोकना है , जिससे मुकदमे का अंतिम परिणाम प्रभावित हो सकता है।
- यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि किसी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति में हित प्राप्त करने वाले तीसरे पक्ष को उस मुकदमे के परिणाम से बाध्य होना चाहिए।
लिस पेंडेन्स सिद्धांत के आवश्यक तत्व (Essential of Lis Pendens)
धारा 52 के प्रावधान लागू होने के लिये निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है[3]:
1. किसी वाद या कार्यवाही का लम्बित होना (Pendency of a suit or proceeding)
विचाराधीन वाद का सिद्धान्त तभी लागू होता है जब वाद या कार्यवाही लम्बित हो। प्रश्न उठता है वाद या कार्यवाही को कब लम्बित माना जायेगा? यह सभी विरोधाभास प्रीवी कौंसिल के फैयाज हुसैन खान बनाम प्राग नारायण[4] नामक वाद में निर्णय के द्वारा समाप्त हुआ। कृष्णन बनाम शिवप्पा[5]' नामक वाद में यह और भी स्पष्ट हो गया जब सर लारेन्स ने कहा कि धारा में प्रयुक्त शब्द 'प्रतिविरोधात्मक' से यह माना जाना चाहिए कि वाद वास्तविक है न कि दुरभि संधि का परिणाम।
'किसी बाद या कार्यवाही का लम्बन इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस तारीख से प्रारम्भ हुई समझ जायेगा जिस तारीख को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में वह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया या वह कार्यवाही संस्थित की गई और बाद या कार्यवाई तब तक लम्बित या चलता हुआ माना जायेगा जब तक उस वाद या कार्यवाई का निपटारा अन्तिम डिक्री या आदेश द्वारा न हो गया हो और ऐसी डिक्री या आदेश की पूरी तुष्टि न प्राप्त कर ली गई हो।'
2. वाद या कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में लम्बित होना चाहिए
विचाराधीन वाद का सिद्धान्त न केवल लम्बित वाद पर लागू होता है अपितु लम्बित कार्यवाही पर भी लागू होता है। धारा 52 के प्रयोजन के लिए वाद और कार्यवाही में कोई अन्तर नहीं है। कार्यवाही का तात्पर्य होता है एक विधिक प्रक्रिया या न्यायालय के प्राधिकार से किया गया कोई कार्य। इस धारा का प्रयोग उन अन्तरणों पर भी किया गया जो राजस्व कार्यवाहियों के दौरान भी किया गया है[6]।
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 58 के अन्तर्गत कुर्क की गई सम्पत्ति पर दावों का और ऐसी सम्पत्ति के कुर्की के बारे में आक्षेपों के न्याय निर्णयन सम्बन्धी कार्यवाही भी धारा 52 की परिधि में आती है। इसी तरह राजस्व अधिकारी के समक्ष बेदखली की कार्यवाही भी विचाराधीन वाद के सिद्धान्त से प्रभावित होती है[7]।
3. बाद या कार्यवाही दुस्संधिपूर्ण न हो
विचाराधीन वाद के सिद्धान्त के लागू होने के लिए तीसरी शर्त यह है कि वाद या कार्यवाही दुस्संधिपूर्ण न हो या दुरभिसंधि का परिणाम न हो। एक दुस्संधिपूर्ण वाद वास्तविक वाद नहीं है। यह पक्षकारों के बीच एक लड़ाई नहीं अपितु छद्म युद्ध (sham fight) है[8]। विधिक कार्यवाहियों में दुस्संधि को ह्वारटन्स ला लेक्सिकन (Wharton's Law Lexicon) 14वें सन्सकरण, पृ० 212 पर परिभाषित किया गया है-
'विधिक कार्यवाहियों में दुस्संधि दो व्यक्तियों के बीच एक गुप्त व्यवस्था है कि एक व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध किसी अहितकारी को लेकर वाद संस्थित करेगा ताकि न्यायिक अभिकरण का निर्णय प्राप्त किया जा सके।'
नागूबाई बनाम बी० शाम राव[9] के वाद में उच्चतम न्यायालय ने दुस्संधिपूर्ण वाद की व्याख्या करते हुए कहा कि इसमें दावा काल्पनिक (बनावटी) होता है, विवाद अवास्तविक है और डिक्री मात्र एक मुखौटा है। एक कपटपूर्ण वाद के बारे में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसमें दावा असत्य होता है और दावेदार धोखाधड़ी करके न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त करता है। इसमें लड़ाई वास्तविक होती हैं, गंभीर होती है।
4. ऐसे वाद या कार्यवाही में स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई अधिकार प्रत्यक्षतः एवं विनिर्दिष्टत प्रश्नगत हो (Right to immovable property should be directly and specifically in question)
धारा के प्रावधानों को लागू होने के लिए यह चौथी शर्त है कि ऐसे वाद या कार्यवाही में स्थावर (अचल) सम्पत्ति में सम्बन्धित कोई अधिकार प्रत्यक्षतः एवं विनिर्दिष्टतः प्रश्नगत हो[10]। यह धारा अभिव्यक्त रूप से विचाराधीन वाद के सिद्धान्त को उन स्थावर सम्पत्तियों तक सीमित करती है जो भारतवर्ष में स्थित है, भारतवर्ष के बाहर नहीं[11]। अचल सम्पत्ति से सम्ब न्धत कोई अधिकार प्रत्यक्षतः एवं विनिर्दिष्टतः प्रश्नगत निम्न प्रकार के वादों में माना गया है-
- अचल सम्पत्ति के अन्तरण की संविदा से सम्बन्धित विनिर्दिष्ट पालन (specific performance) का वाद[12];
- बन्धक से सम्बन्धित एक वाद[13];
- एक अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित विभाजन का वार्ड[14],
- हकशुफा का एक वाद[15];
- बन्धक ऋण के अंशदान के लिए एक वाद[16];
- न्यास विलेख के निरस्त करने सम्बन्धी वाद जिसमें अचल सम्पत्ति के पुनः हस्तान्तरण की माँग की गई है[17]।
5. विवादित सम्पत्ति मुकदमें के किसी पक्षकार द्वारा अन्तरित होनी चाहिए या अन्यथा व्ययनित होनी चाहिए
विचाराधीन वाद के सिद्धान्त के लागू होने के लिए पाँचवां आवश्यक तत्व है कि सम्पत्ति वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा अवश्य अन्तरित की जानी चाहिए। या अन्यथा व्ययनित (disposed of) होनी चाहिए[18]। अतः जहाँ सम्पत्ति का अन्तरण एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसका स्वत्व वाद के पक्षकारों से सर्वोपरि है या जिसका स्वत्व उनसे किसी भी प्रकार सम्बन्धित नहीं है वहाँ ऐसा अन्तरण विचाराधीन वाद के सिद्धान्त से प्रभावित नहीं होगा। इसी प्रकार सिद्धान्त वहाँ भी नहीं लागू होगा जहाँ वाद के लम्बित रहते हुए सम्पत्ति का अन्तरण एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो अन्तरण के समय वाद का पक्षकार नहीं था परन्तु जो मूल प्रतिवादी के प्रतिनिधि के रूप में वाद में पक्षकार बना[19] । जहाँ एक विक्रय का करार तीसरे पक्ष में संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिये वाद संस्थित करने से पूर्व निष्पादित किया गया वहाँ जैसा कि केरल उच्च न्यायालय ने राजन बनाम यूनुस कुट्टी[20] में अभिनिर्धारित किया, ऐसा करार विचाराधीन वाद के सिद्धान्त से बाधित नहीं है।
6. ऐसे अन्तरण से दूसरे पक्षकार का अधिकार प्रभावित होना चाहिए
धारा 52 के प्रावधानों को लागू होने के लिए छीं और अन्तिम शर्त यह है कि अन्तरण के बाद के दूसरे पक्षकार का अधिकार अवश्य प्रभावित होना चाहिए[21]। 'किसी अन्य पक्षकार' से तात्पर्य कोई अन्य पक्षकार जिसके और अन्तरण करने वाले पक्षकार के बीच निर्णय के लिए विवाद्यक (issue) है जिस पर अन्तरण से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा[22]। दूसरे शब्दों में 'किसी अन्य पक्षकार' से तात्पर्य अन्तरक के अलावा एक पक्षकार। अन्तरक और उसके प्रतिनिधि इस सिद्धान्त का अवलम्ब अन्तरिती के विरुद्ध नहीं ले सकते। विचाराधीन वाद का सिद्धान्त वहाँ नहीं लागू होता जहाँ पक्षकार उसी तरफ (पक्ष) के हों चाहे वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में। यह धारा वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ केवल अन्तरक का अधिकार प्रभावित होता है, वाद के किसी अन्य पक्षकार का नहीं सिद्धान्त का उद्देश्य सिर्फ मुकदमें के पक्षकारों को सुरक्षा प्रदान करना है, उनके विरोधियों द्वारा किये गये अन्तरण के विरुद्ध ।
लिस पेंडेंस के सिद्धांत की प्रयोज्यता (Applicability of Doctrine of Lis Pendens) - सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 52 के अंतर्गत लिस पेंडेंस के नियम की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक तत्व बताए हैं। वे इस प्रकार हैं:
- मुकदमा कार्यवाही में होना चाहिए .
- दायर किया गया वाद सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत में दायर किया जाना चाहिए।
- अचल संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार प्रत्यक्षतः और विशिष्ट रूप से प्रश्नगत है।
- यह मुकदमा सीधे तौर पर दूसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करता है।
- प्रश्नगत संपत्ति किसी भी पक्ष द्वारा हस्तांतरित की जा रही है ।
- वाद कपटपूर्ण (ऐसा वाद जिसमें धोखाधड़ी या कपट से डिक्री प्राप्त की गई हो) प्रकृति का नहीं होना चाहिए ।
सिद्धांत की अप्रयोज्यता (Non- Applicability of Doctrine of Lis Pendens) : यह सिद्धांत कुछ मामलों में लागू नहीं होता है। वे इस प्रकार हैं:
- विलेख के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में बंधककर्ता द्वारा की गई बिक्री।
- ऐसे मामलों में जहां केवल हस्तान्तरणकर्ता ही प्रभावित होता है ।
- ऐसे मामलों में जहां कार्यवाही प्रकृति में कपटपूर्ण हो।
- जब संपत्ति का वर्णन सही ढंग से नहीं किया गया हो और उसकी पहचान न हो सके।
- जब उक्त संपत्ति पर अधिकार सीधे तौर पर प्रश्नगत न हो और हस्तांतरण की अनुमति हो।
निष्कर्ष
संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद, यह निष्कर्ष निकालता है, कि लिस पेंडेंस के सिद्धांत को लागू करने के लिए, मुकदमा एक अचल संपत्ति के संबंध में होना चाहिए जिसमें महत्वपूर्ण रूप से इसके अधिकारों के बारे में प्रश्न शामिल हों ओर यह सुनिश्चित करता है कि सिद्धांत को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब ऐसी शर्तें पूरी की जाती हैं। केवल वादपत्र में अचल संपत्ति का उल्लेख करके किसी के द्वारा इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।
दूसरे शब्दो में, यह सिद्धांत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान स्थानांतरण पर रोक लगाता है। यह वादी को इस हद तक सुरक्षा प्रदान करता है कि यदि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान स्वामित्व की कोई बिक्री या हस्तांतरण किया जाता है, तो ऐसी कोई भी कार्रवाई अमान्य हो जाएगी और क्रेता मुकदमे के परिणाम से बाध्य हो जाएगा। एक तरह से, जो ब्याज अन्यथा क्रेता के लिए निहित प्रकृति का होता, वह तब आकस्मिक हित बन जाता है जब कोई हस्तांतरण पेंडेंट लाइट में किया जाता है।
[1]. (1857) 1 डे० जी० एण्ड जे० 566.
[2]. एन० सी० भारतीय बनाम गंगा देवी पीपुल्स को० बैंक लि० ए० आई० आर० 2002 गुज० 209; संजय.
[3]. कृष्नप्पा बनाम शिवप्पा, (1907) 31 बाम्बे 393.
[4]. (1907) 29 इला० 339 (345).
[5]. (1907) 31 बाम्बे 393.
[6]. मनोहर एवं चिताले , वही वाल्यूम 2 पृष्ठ 14.
[7]. जयराम बनाम मईफुजाली, ए० आई० आर० 1948 नाग० 283.
[8]. अहमद भाय बनाम बल्ली भाय, (1882) 6 बाम्बे 703.
[9]. ए० आई० आर० 1956 सु० को० 593 ($598).
[10]. जयनल आवेदीन बनाम हैदरअली खान, ए० आई० आर० 1928 कल० 441.
[11]. शिवारामाकृष्णा बनाम मम्मू, ए० आई० आर० 1957 मद्रास 214.
[12]. गौरीदत्त महाराज बनाम सुकुर मोहम्मद, ए० आई० आर० 1948 पी० सी० 141.
[13]. .फैयाज हुसैन खान बनाम प्राग नारायन, (1907) 29 इला० 339.
[14]. .जयराम मुदालियर बनाम अय्यास्वामी, ए० आई० आर० 1973 सु० को० 569.
[15]. माधो सिंह बनाम स्कीनर, ए० आई० आर० 1941 लाहौर 433.
[16]. जमना देवी बनाम मंगल दास, ए० आई० आर० 1946 पट० 306.
[17]. भोला नाथ बनाम भूतयान, ए० आई० आर० 1925 कल० 239.
[18]. कस्तूरी देवी बनाम हरवन्त सिंह, ए० आई० आर० 2000 पं० एण्ड हरि० 271,
[19]. .बाला रामाभद्रा बनाम दठलू, 27 बाम्बे, एल० आर० 38.
[20]. ए० आई० आर० 2002 केरल 339.
[21]. ऊषा रानी वानिक बनाम हरिदास दास, ए० आई० आर० 2005 गुवा० 1.
[22]. कृष्णैया बनाम मलैय्या, (1918) 41 मद्रा० 458.